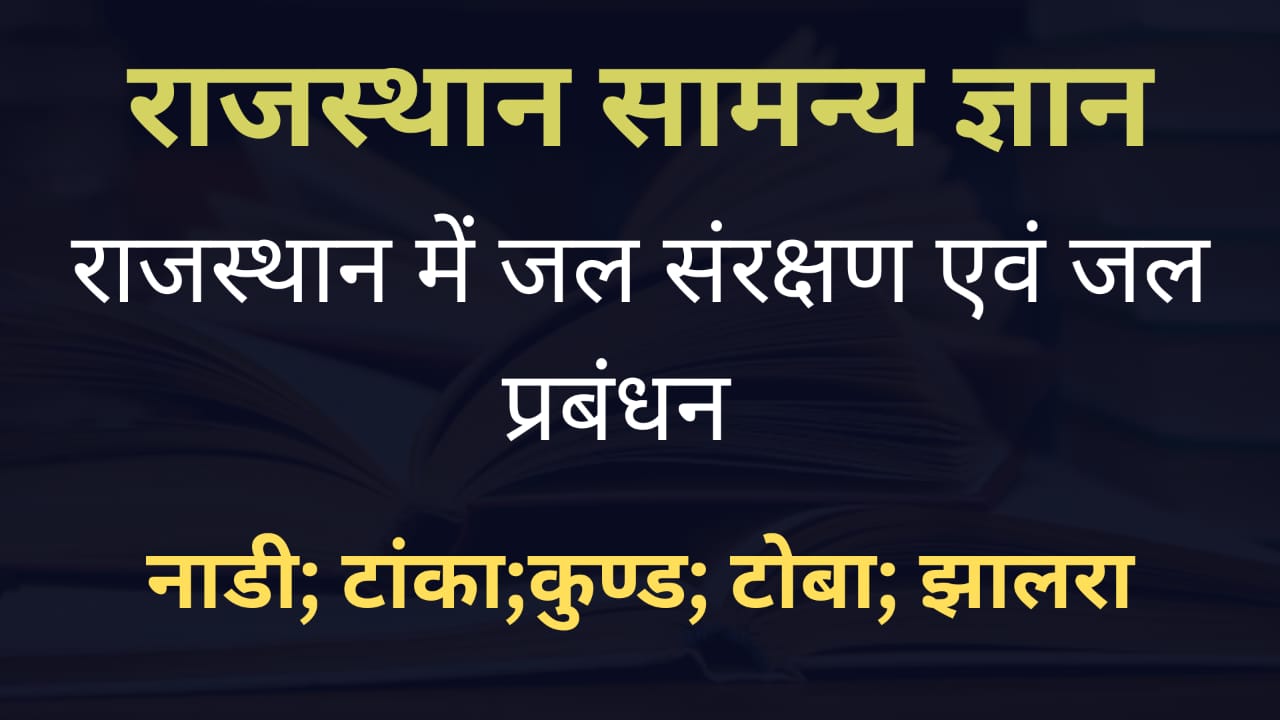राजस्थान मे जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन
जल संरक्षण – जल का उचित रूप से उपयोग व लम्बे समय तक सुरक्षित रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तान की श्रेणी में आता है। जहाँ वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। जिस कारण राजस्थान के निवासियों ने अपने क्षेत्र के अनुसार जल भण्डारण के विभिन्न ढाचों को अपनाया। इस कारण ही सम्पूर्ण भारत में राजस्थान की जल संग्रहण की विधियां अपना विशेष स्थान रखती है।
राजस्थान में स्थापत्य कला के प्रेमी राजा-महाराजाओं व सेठ साहूकारों ने अपने पूर्वजों की याद में कलात्मक बावड़ियों, कुण्डों, तालाबों व कुओं का निर्माण करवाया।
पश्चिमी राजस्थान में जल को महत्व देते हुए कुछ पक्तियाँ लिखी गई है। जिसमे पानी को घी से भी बढ़कर बताया है। “घी ढूल्यां म्हारो की नीं जासी, पानी ढूल्यां म्हारो जी बले।”
राजस्थान में जल संरक्षण व संग्रहण के परम्परागत स्रोत निम्न प्रकार है –
नाडी – राजस्थान में सबसे पहले पक्की नाडी का निर्माण 1520 ई. मे हुआ, जिसका निर्माण राव जोधाजी ने जोधपुर के निकट करवाया। गाँव के बाहर बनी छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है, वह नाड़ी कहलाती है। यह नाडी गाँव के लोगों की दैनिक जरूरतों को पुरी करती है। अधिकांशत पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गाँव में नाड़ी मिलती है। नाडी के पानी को पालरपाणी के नाम से भी जानते है तथा यह 3 से 12 मीटर तक गहरा होता है। केन्द्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाडमेर व जैसलमेर में पानी की कुल आवश्यकता मे से 37.06% जरुरत नाडियों से से पूरी होती है।
टांका / कुण्ड / कुंडी – राजस्थान के रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाया गया भूमिगत हौद टांका या कुंड कहलाता है। इसको बनाने में चुने व सीमेंट का प्रयोग किया जाता है व उपर से ढक कर छोटी सी खिड़की रखी जाती है। इनका निर्माण खेतों, घरों मंदिरों आदि में करवाया जाता है। इनकी गहराई 40 से 50 फुट तक होती है ।
टोबा – जल का संग्रहण करने की यह विधि नाडी के समान ही होती है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमे पानी का रिसाव बहुत ही कम मात्रा में होता है, वहां टोबा बनाया जाता है सामान्य रूप से टोबा में 7-8 माह तक पानी टहर जाता है। राजस्थान के प्रत्येक गाँव में पशुओं व जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए टोबा का निर्माण किया जाता है।
झालरा – झालरा का कोई जल स्रोत नहीं होता है। बल्कि अपने से ऊँचाई पर स्थित तालाबों / झीलों के रिसाव के पानी को प्राप्त करता है। इसके पानी का उपयोग धार्मिक रीति रिवाज सम्पन्न करने व सामूहिक स्नान आदि कार्यों में किया जाता है। सबसे पहले जोधपुर के महामंदिर के झालरा का निर्माण हुआ ।
आगोर – वर्षा जल को नाडी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर पायतान बनाया जाता है। जिससे पानी बहकर तालाब या नाडी में जाता है।
पायतान – वर्षा जल की टांका था कुण्ड में उतारने के लिए उसके चारों ओर जगह को पक्का कर दिया जाता है उस पक्की भूमि के लिए पायतान शब्द का प्रयोग किया जाता है।
खड़ीन – खड़ीन का प्रचलन सबसे पहले 15 वीं शताब्दी में हुआ खडीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे होता है। जिससे वर्षा का जल बहकर आता हो, खडीन के दोनो तरफ मिट्टी की पाल होती है। वर्षा के समय खड़ीन में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर पानी अगली खडीन में जाता है। जिसके लिए नेहटा मार्ग बनाया जाता है। वर्षा जल सुखने पर नमी युक्त भूमि पर खेती की जाती है वह ‘खडीन कृषि’ कहलाती है। इस तकनीक के माध्यम से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है।
कुएँ या बेरी – छोटा कुआ या कुई को ही मारवाड में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में अधिकांशत्य बेरियां बाडमेर व जैसलमेर में पायी जाती है। बेरी सामान्य रूप से तालाब के समीप बनाई जाती है। जिसमें तालाब का पानी रिसता हुआ एकत्रित हो सके।
जल प्रदूषण – प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल में यदि कुछ अवांछित तत्व मिल जाते है तो यह जल ना तो पीने योग्य होता और न ही मानव के उपयोग के लिए किसी काम का होता है। तो वह जल प्रदूषण कहलाता है।
जल प्रदूषण के कारण –
कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग।
जलाशयों के पास कपड़े धोना व पशुओं को नहलाना।
खुले में शौच कार्य करना ।
घरेलु अपशिष्ट पदार्थी को जल में डालना।
उद्योगों से निकले ठोस अपशिष्ट पदार्थ व रासायनिक तत्वों का जल में घुल मिल जाना।
जल प्रदूषण को रोकने के उपाय –
शहरों के सीवरेज जल को जलाशयों में मिलने से पहले साफ़ करके उसको दुबारा उपयोग योग्य बनाया जाये।
शहरी कचरे को खाली जल स्रोतों में न करके बंजर अनुपयोगी भूमि पर किया जाये।